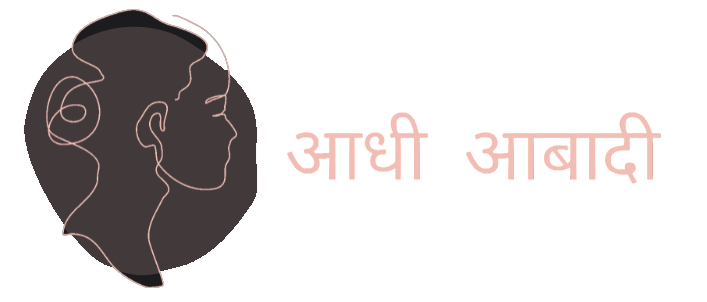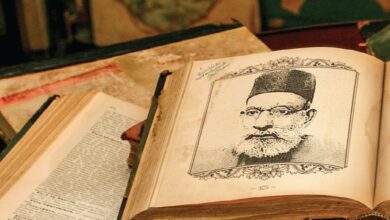“विवाह, धर्म और स्त्री अस्मिता: भारतीय समाज की बदलती संरचना”
"स्त्री के अस्मिता की लड़ाई: विवाह संस्था और पितृसत्ता के बीच संघर्ष"

हिंदू धर्म जिस भारतीय समाज में प्रचलित है, वह एकरूप नहीं बल्कि विविध रूपों वाला है। इसकी संरचना विषम है और इसमें कई परतें हैं। चार वर्गों की जाति-व्यवस्था सैकड़ों जातियों में विभाजित है। हिंदू धर्म की मूल मान्यताएं और उपासना पद्धतियां स्त्री-पुरुष तथा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न और सापेक्ष होती हैं, जिन पर विशेष रूप से वर्चस्वशाली वर्ग का अधिकार होता है।
धर्म एक राजनीतिक उपक्रम भी होता है, इसलिए इस पर सामाजिक नियंत्रण भी कायम रहता है। जैसे घर में परिवार का मुखिया धर्माचरण को नियंत्रित करता है, वैसे ही समुदाय में यह भूमिका धर्माचार्य निभाते हैं और निम्न वर्गों के धर्म-व्यवहार पर सवर्णों का नियंत्रण होता है।
यह सर्वविदित है कि स्त्री का धर्माचरण पुरुषों के अनुकरण में होता है। स्त्रियों को वे सभी परंपराएं स्वीकार करनी पड़ती हैं जो पुरुष वर्ग के हित में हों।
स्त्री-समकक्षता से पुरुषों की असहजता
पिछले कुछ दशकों में समाज में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आए हैं। एक ओर जहां स्त्री शिक्षा और समान अधिकारों की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर दहेज, हिंसा और भ्रष्टाचार में भी वृद्धि हुई है। यदि इन परिवर्तनों को स्त्री-पुरुष संबंधों के संदर्भ में देखा जाए तो “अहं” का टकराव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
स्त्रियां अब अपनी अस्मिता की तलाश में हैं और पुरुषों के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को चुनौती दे रही हैं। वर्तमान पीढ़ी की महिलाएं अपनी प्राथमिकताओं को लेकर क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं। उनकी समकक्षता का दावा पुरुषों के लिए असहज अनुभव बन जाता है, और यहीं से अहंकार की टकराहट शुरू होती है।
आज की युवतियां समझ चुकी हैं कि स्त्री धर्म की अवधारणा नैतिकता और भय के जाल में उन्हें जकड़ चुकी है। इसी कारण वे पति और परिवार के लिए अपनी अस्मिता के बलिदान को कर्तव्य समझती आई हैं।
स्त्री जीवन की आचार संहिता प्रारंभ से ही पक्षपातपूर्ण रही है। वर्चस्ववादी परंपराएं और संस्कार स्त्रियों के स्वाभाविक विकास में बाधा बनते आए हैं। विवाह संस्था को भी इस प्रक्रिया का एक अहम माध्यम माना गया है। विवाह एक ऐसा ढांचा बन गया है जो स्त्री की देहगत पवित्रता की जिम्मेदारी लेता है और उसके मानसिक स्वतंत्रता को नियंत्रित करता है।
विवाह के नाम पर वैधानिक शोषण की परंपरा चलती रही है, जिससे स्त्री की वैचारिक अस्मिता क्षीण हो जाती है।
विवाह संस्था पर युवा पीढ़ी का अविश्वास

आज की युवा पीढ़ी विवाह संस्था पर संदेह करने लगी है। वे इसके औचित्य को लेकर संशय में हैं और इस परंपरा को तोड़ने के प्रयास कर रही हैं। विवाह के अंतर्गत स्त्री की स्वाभाविक प्रकृति को दबा दिया जाता है। समाज ने प्रेम को विवाह की स्वीकृति से जोड़ दिया है, जबकि अधिकतर विवाह आज भी प्रेम पर आधारित नहीं होते।
नारीवादियों का यह तर्क महत्वपूर्ण है कि पुरुषवादी समाज में विवाह के बाद भी स्त्री-पुरुष के बीच बनने वाले अनैच्छिक संबंधों को बलात्कार की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। हालांकि भारतीय समाज में पति को परमेश्वर माना गया है, और उसकी इच्छा को नारी धर्म का हिस्सा माना जाता है।
शिक्षा और चेतना के चलते आज की युवतियों में विवाह को लेकर भय और असमंजस है। पुरुषों को परिवार में स्वतंत्रता प्राप्त होती है, पर स्त्री को पति, बच्चों और घर की अन्य महिलाओं के दबावों का भी सामना करना पड़ता है।
प्रेम और मानसिक सामंजस्य
यदि विवाह में प्रेम होता तो स्त्री को इन विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। विवाह एक सामाजिक समझौता है, जबकि प्रेम स्वाभाविक भावना है। इसलिए परिवार में विवाह और प्रेम का सामंजस्य अक्सर असंतुलित दिखाई देता है।
प्रेम-विवाह संभव है, लेकिन वह तभी सफल होता है जब पुरुष स्त्री की इच्छाओं और भावनाओं को समझे और उन्हें प्राथमिकता दे। हमारे समाज में ऐसे उदाहरण हैं, पर उनकी संख्या अभी सीमित है।
विवाह के बाद का प्रेम अक्सर कृत्रिम होता है, जो केवल शारीरिक संबंधों पर आधारित होता है। जबकि सच्चा प्रेम मानसिक मेल पर निर्भर करता है।
पति अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए पत्नी को अपनी संपत्ति मानता है, जिससे संबंधों में प्रेमिका-पति की भूमिका विकसित नहीं हो पाती।
आर्थिक स्वावलंबन और विवाह संस्था
वर्तमान में विवाह संस्था के नैतिक मानदंडों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। आर्थिक स्वावलंबन ने युवक-युवतियों को विवाह से दूर किया है और वे इसे नैतिकता के संकट के रूप में देखने लगे हैं।
सामाजिक सोच में बदलाव ने परिवार संस्था को भी प्रभावित किया है। आज की पीढ़ी विवाह को लेकर दुविधा में है। विवाह संस्था तभी सुरक्षित रह सकती है जब उसमें विवेक और आपसी समझ हो।
प्रेम-विवाह और अंतर्जातीय विवाह की संख्या बढ़ रही है, फिर भी प्रेम को समाज में अनैतिक और विवाह को नैतिक माना जाता है। विवाह के बाद स्वाभाविक प्रेम तभी विकसित हो सकता है जब दोनों का मानसिक स्तर समान हो।
यह वेबसाईट आपके ही सहयोग से चलती है।
वेबसाइट को SUBSCRIBE करके
भागीदार बनें।

डॉ. आकांक्षा मूलत: बिहार की रहने वाली हैं. इन्होने महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) से स्त्री अध्ययन विषय में एम.ए., एम.फिल. (स्वर्ण पदक) एवं डाक्टोरेट की डिग्री प्राप्त की हैं. मुख्यतौर पर जेंडर, ‘गांधी एवं अन्य सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से लेखन – कार्य. अबतक कई प्रतिष्ठित समाचारपत्र, पत्रिकाओं, किताबों एवं आनलाईन पोर्टल्स पर इनके आलेख प्रकाशित हो चुके हैं. स्त्री मुद्दों पर युवा लेखन के लिए “गोदावरी देवी सम्मान” से सम्मानित. विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ जेंडर आधारित मुद्दों पर कार्य. स्त्री अध्ययन विभाग वर्धा एवं स्त्री अध्ययन केंद्र, पटना विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य. ‘गांधीयन सोसाइटी’ न्यू जर्सी अमेरिका एवं इंडिया द्वारा डॉ. एस. एन. सुब्बाराव फेलोशिप कार्यक्रम में फेलो के तौर पर कार्यानुभव.