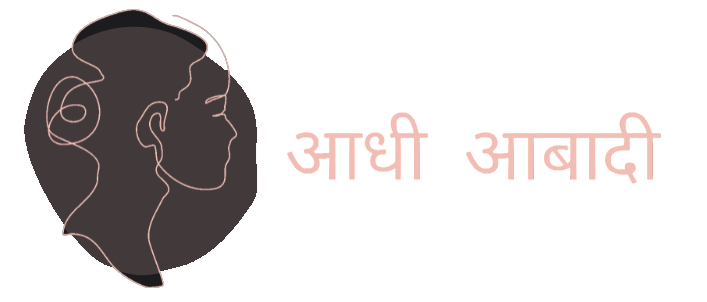क्या लड़कियाँ सच में डिजिटल रूप से आज़ाद हैं?
भारत में डिजिटल शिक्षा की पहुंच से वंचित लड़कियाँ – क्या तकनीक से बराबरी अब भी एक सपना है?

कनाडाई संचार सिद्धांतकार मार्शल मैकलुहान (Marshall McLuhan) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Understanding Media: The Extensions of Man के पहले अध्याय में लिखा था, “The medium is the message”, अर्थात् माध्यम ही संदेश होता है।
सही सूचना अगर सही समय पर लोगों तक पहुँचती है, तो यह अवसर उत्पन्न करती है, जो समाज में क्रांति का आह्वान करती है। लेकिन ‘माध्यम’ तभी क्रांति का साधन बन सकता है, जब समाज उसे खुले मन से स्वीकारे। यह तभी संभव है जब समाज लोकतांत्रिक हो, लैंगिक दृष्टिकोण से निष्पक्ष हो, और ‘माध्यम’ केवल एक वर्ग तक सीमित न रह जाए।
समाज को माध्यम की उपयोगिता का भान नहीं
यहां ‘माध्यम’ का तात्पर्य उन तकनीकी साधनों से है, जो लोगों को जोड़ते हैं—जैसे रेडियो, टीवी, स्मार्टफोन आदि। दुर्भाग्यवश भारत जैसे देश में सूचना का उद्देश्य शिक्षा और जागरूकता की बजाय अधिकांशतः मनोरंजन रह गया है, और वह भी उन्हीं वर्गों के लिए, जिन्हें इसकी पहुँच उपलब्ध है।
टीवी और रेडियो पर पहले भी शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित होते थे—जैसे ‘युवावाणी’—और आज भी होते हैं, लेकिन यह लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है जो इसकी उपयोगिता को समझते हैं।
वहीं, जो वर्ग दो वक़्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके लिए महंगे रिचार्ज और इंटरनेट खर्च के बीच ऑनलाइन शिक्षा एक लग्ज़री बनकर रह जाती है।
ऑनलाइन पढ़ाई: लड़कियों के लिए एक सपना
ऑनलाइन शिक्षा भविष्य का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। कोरोना काल में भारत में जब शिक्षा को डिजिटल स्वरूप दिया गया, तब लड़कियों के लिए पढ़ाई जारी रखना एक बड़ी चुनौती बन गया। ‘
The Mobile Gender Gap Report 2019’ के अनुसार भारत में केवल 35% महिलाओं के पास इंटरनेट की सुविधा है। संचार का माध्यम अब भी महिलाओं के लिए सीमित है।
COVID-19 से पहले भारत में करीब 30 मिलियन स्कूल जाने वाले बच्चे थे, जिनमें से 40% किशोरियाँ थीं। इनमें अधिकांश के पास ऑनलाइन पढ़ाई के संसाधन नहीं थे। आज भी कई लड़कियों के लिए स्क्रीन पर पढ़ाई करना केवल एक सपना है।
एक सर्वे से खुली सच्चाई
इस मुद्दे पर मैंने बिहार के विभिन्न सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं के घर कॉल किया, यह जानने के लिए कि उनके लिए संचार का माध्यम कितना स्वतंत्रतादायक है।
अधिकतर मामलों में कॉल उनके पिता या भाई ने उठाया। जब उनसे छात्रा से बात कराने की बात की गई, तो अधिकतर ने कहा, “आप हमसे ही बात कर लीजिए।”
जब मैंने पूछा कि बेटी या बहन किस तरह से पढ़ाई करती है, तो जवाब मिला, “फोन देने से क्या फ़ायदा? उसे कॉल लगाना भी नहीं आता। बस नंबर याद रहता है।” ऐसे जवाबों के बाद पूछने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं।
कब आएगी डिजिटल आज़ादी?
कुछ लड़कियों से जब सीधे बात हो पाई, तो उन्होंने कहा, “दीदी, ज़्यादा देर बात नहीं कर सकते, घरवाले सवाल करने लगते हैं।” कईयों ने बताया कि उन्हें फोन पर बात करते देख मां-बाप या भाई स्क्रीन में झांकने लगते हैं। कुछ ने कहा कि भाई को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फोन दिया जाता है, उन्हें नहीं।
अधिकांश घरों की यही स्थिति है। हालांकि जिनके अभिभावक थोड़े लिबरल हैं, वहाँ स्थिति कुछ हद तक बेहतर है। इस सर्वे से यह स्पष्ट हुआ कि भारत में लड़कियों की डिजिटल स्वतंत्रता को कई आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियाँ रोक रही हैं।
भारत भले ही 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा हो, लेकिन अभी भी लाखों लड़कियाँ फोन छूने और ऑनलाइन पढ़ाई की आज़ादी से वंचित हैं।
पहले रेडियो को क्रांति का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता था—जैसा कि Amazon Mini Movie ‘Transistor‘ में दिखाया गया है। फिर टीवी आया, अब स्मार्टफोन। लेकिन लड़कियों को अब भी इन ‘माध्यमों’ के प्रयोग की स्वतंत्रता नहीं है।
डिजिटल स्वतंत्रता की बाधाएँ
सरकारें भले ही योजनाएँ लाती हों, लेकिन उनकी नींव अक्सर खोखली होती है। लड़कियों के डिजिटल सशक्तिकरण में प्रमुख बाधाएँ हैं:
-
सामाजिक मानसिकता: कई लोग लड़कियों के फोन इस्तेमाल को बुरा मानते हैं। उन्हें लगता है कि फोन पर मुस्कुराती या टाइप करती लड़कियाँ ‘बिगड़’ रही हैं।
-
भाषाई अवरोध: ज़्यादातर डिजिटल इंटरफेस अंग्रेज़ी में होते हैं, जिससे गाँव और कम पढ़ी लड़कियाँ वंचित रह जाती हैं।
-
बिजली की असमान आपूर्ति: ‘सौभाग्य योजना’ भले ही 99% बिजली उपलब्ध होने का दावा करती हो, लेकिन मिशन अंत्योदय के अनुसार केवल 47% घरों को 12 घंटे से ज़्यादा बिजली मिलती है। बिजली नहीं होगी तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी?
समाधान: सूचना का स्वतंत्र उपयोग
इस खाई को पाटने के लिए जरूरी है कि:
-
अभिभावकों की काउंसलिंग की जाए ताकि वे लड़कियों को तकनीक के इस्तेमाल की अनुमति दें।
-
आर्थिक सशक्तिकरण से सामाजिक सोच बदली जा सकती है।
-
लड़कियों को न सिर्फ़ सूचना का अधिकार मिले, बल्कि उसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का भी अवसर दिया जाए।
“मुट्ठी” अब भी छोटी है
समय के साथ स्वतंत्रता के मायने बदलते हैं। कोरोना ने यह सिखाया कि केवल साइकिल और पैसे देना लड़कियों को आत्मनिर्भर नहीं बनाता। बल्कि उन्हें बदलते ज़माने के अनुरूप तकनीकी तौर पर सशक्त करना ज़रूरी है।
रिलायंस ने कभी कहा था, “कर लो दुनिया मुट्ठी में”। लेकिन यह मुट्ठी लड़कियों के लिए अब भी बहुत छोटी है। जब तक उन्हें माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक उनकी दुनिया मुट्ठी में नहीं आएगी—बल्कि और सीमित हो जाएगी।
यह वेबसाईट आपके ही सहयोग से चलती है।
वेबसाइट को SUBSCRIBE करके
भागीदार बनें।
मेरी कलम मेरे जज़्बात लिखती है, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, उनके अल्फाज़ लिखती है। Received UNFPA-Laadli Media and Advertising Award For Gender Senstivity -2020 Presently associated with THIP- The Healthy Indian Project.