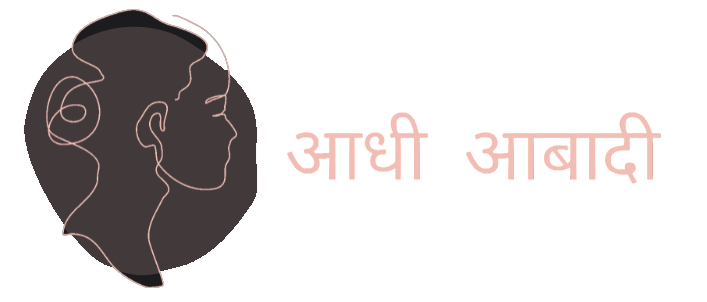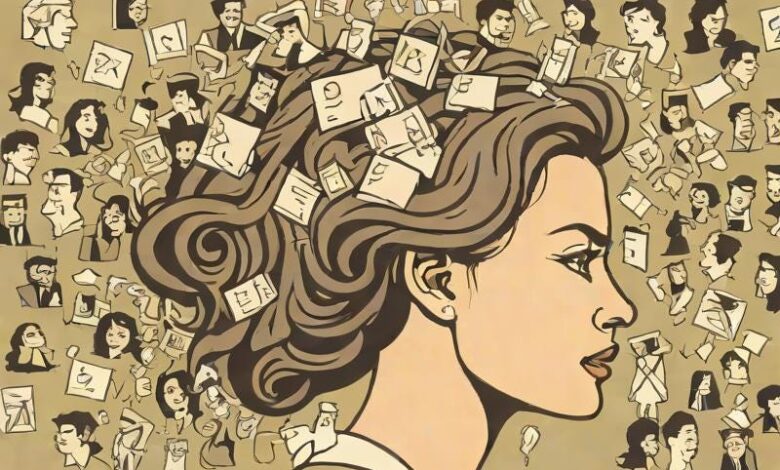
हमारे समाज में आज भी अकेली स्त्री का अस्तित्व ‘अप्राकृतिक’ माना जाता है। ऐसी स्त्री, जो विवाह संस्था से अलग रहकर अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ जीवन जीना चाहती है, समाज की दृष्टि में संदेहास्पद बन जाती है। यह अकेली स्त्री अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा कोई भी हो सकती है। उसके अपने घर की कल्पना तक नहीं की जाती।
न तो उसे अकेले घर में रहने की अनुमति मिलती है और न ही समाज में स्वतंत्र जीवन जीने की। अगर कोई स्त्री इस तरह की जिंदगी चुनती है, तो इसे समाज, परिवार और स्वयं उस स्त्री के लिए ‘अपमानजनक’ माना जाता है।
समाज और राज्य किसी महिला को तभी ‘आदर्श’ मानते हैं, जब वह अपने अधिकार, सम्मान, निर्णय लेने की क्षमता और यहां तक कि अपना शरीर भी किसी पुरुष को सौंप देती है। यह एक गहरी पितृसत्तात्मक मानसिकता को दर्शाता है, जो स्त्री को एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं, बल्कि ‘रक्षिता’ के रूप में ही स्वीकार करता है। मध्यमवर्गीय समाज आज भी खुद को मनुवादी सोच से पूरी तरह अलग नहीं कर पाया है।
“क्या अकेली महिला होना अपराध है?”

फिर भी, हाल के वर्षों में मध्यमवर्ग की लड़कियां और महिलाएं चुनौतियों के बावजूद इंसान के रूप में अपनी सामाजिक पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वे समझने लगी हैं कि उनकी दोयम दर्जे की स्थिति का एक बड़ा कारण सत्ता और संसाधनों पर उनका नियंत्रण न होना है। आर्थिक स्वतंत्रता इस नियंत्रण का सबसे अहम पहलू है, जिससे अधिकांश महिलाएं वंचित हैं। कई महिलाएं परिस्थितियों को समझने के बावजूद, पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और मूल्यों को ढोती रहती हैं।
इस सामाजिक conditioning की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है, जब दादी-नानी या मां लड़कियों को यह सिखाती हैं कि उन्हें कैसे बोलना, चलना, हंसना और ‘परिवार की इज्जत’ बनाए रखना है।
विवाह संस्था को एक ‘करियर’ की तरह प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें प्रवेश करने के बाद स्त्री को खुद के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं रहती। निर्णय लेने की जिम्मेदारी उस पुरुष पर डाल दी जाती है, जिससे उसका विवाह होता है। विवाह स्त्री को रोटी, कपड़ा और छत देता है, लेकिन बदले में उसका आत्मबल, उसका शरीर और उसकी स्वतंत्रता छीन लेता है।
यही कारण है कि कई शिक्षित और स्वावलंबी महिलाएं भी जीवनभर पिता, पति और फिर पुत्र पर निर्भर रहती हैं। वे मानसिक रूप से इतनी आदी हो जाती हैं कि उन्हें अपनी स्वतंत्रता में भी असुरक्षा महसूस होती है।
जिन महिलाओं के पास आय के साधन हैं, उनमें से भी अधिकांश के पास उस कमाई के उपयोग पर पूरा नियंत्रण नहीं होता। आत्मबल के अभाव के कारण वे यह निर्णय नहीं ले पातीं कि अपनी कमाई को कहां और कैसे खर्च करें। उन्हें यह मानने के लिए प्रशिक्षित किया गया है कि पैसे और जीवन से जुड़े बड़े निर्णय पुरुष ही लेंगे, जबकि उनकी ‘प्राकृतिक’ जिम्मेदारी केवल परिवार, बच्चों और पति की देखभाल करना है। यदि कोई महिला आत्मनिर्भर बनना भी चाहती है, तो उसे अपने पारंपरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए ही आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है।
यह विडंबना ही है कि जीवन का जो समय करियर निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, वही समय स्त्रियों के लिए प्रजनन और पालन-पोषण के दायित्वों से जुड़ा होता है। जब पुरुष अपने करियर में आगे बढ़ रहे होते हैं, तब महिलाएं गर्भधारण, प्रसव और पालन-पोषण में व्यस्त रहती हैं। नतीजतन, वे करियर की दौड़ में पीछे छूट जाती हैं। विवाह के बाद स्त्री की क्षमता, योग्यता और महत्वाकांक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता।
“जब स्त्री अपनी पहचान खुद गढ़ना चाहती है”

यदि कोई अकेली स्त्री या तलाकशुदा महिला इन परंपराओं को तोड़कर अपनी पहचान बनाना चाहती है, तो समाज और राज्य दोनों उसे रोकने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। क्योंकि ऐसी महिलाएं किसी पुरुष की ‘रक्षिता’ नहीं होतीं, उनकी यौनिकता पर कोई अधिकृत नियंत्रण नहीं होता — यह बात समाज को असहज करती है।
लड़कियों के मामले में परिवार की ‘इज्जत’, ‘शुद्धता’ और ‘नारी शुचिता’ जैसी अवधारणाएं यौन नियंत्रण से जुड़ी होती हैं। जबकि पुरुषों के मामले में ऐसे सामाजिक दबाव नहीं होते।
विधवा या तलाकशुदा महिलाओं की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। उन पर न केवल घर और परिवार का नैतिक दबाव होता है, बल्कि समाज का कठोर दृष्टिकोण भी उन पर हावी रहता है। चाहे वे घर में हों या कार्यक्षेत्र में, हर समय उन पर यह सामाजिक नियंत्रण बना रहता है कि वे किसी पुरुष के साथ अपनी मर्जी से न तो शारीरिक संबंध बना सकती हैं, न ही बिना विवाह के संतानोत्पत्ति कर सकती हैं।
स्त्री की यौनिकता पर यह नियंत्रण विवाह संस्था में केवल पति तक सीमित होता है, लेकिन जैसे ही वह विवाह संस्था से बाहर होती है, यह नियंत्रण पूरे समाज का बन जाता है। यह समाज स्त्री को उसके शरीर, विचार और निर्णयों पर अधिकार देने के लिए अब भी तैयार नहीं है।
यह वेबसाईट आपके ही सहयोग से चलती है।
वेबसाइट को SUBSCRIBE करके
भागीदार बनें।

डॉ. आकांक्षा मूलत: बिहार की रहने वाली हैं. इन्होने महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) से स्त्री अध्ययन विषय में एम.ए., एम.फिल. (स्वर्ण पदक) एवं डाक्टोरेट की डिग्री प्राप्त की हैं. मुख्यतौर पर जेंडर, ‘गांधी एवं अन्य सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से लेखन – कार्य. अबतक कई प्रतिष्ठित समाचारपत्र, पत्रिकाओं, किताबों एवं आनलाईन पोर्टल्स पर इनके आलेख प्रकाशित हो चुके हैं. स्त्री मुद्दों पर युवा लेखन के लिए “गोदावरी देवी सम्मान” से सम्मानित. विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ जेंडर आधारित मुद्दों पर कार्य. स्त्री अध्ययन विभाग वर्धा एवं स्त्री अध्ययन केंद्र, पटना विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य. ‘गांधीयन सोसाइटी’ न्यू जर्सी अमेरिका एवं इंडिया द्वारा डॉ. एस. एन. सुब्बाराव फेलोशिप कार्यक्रम में फेलो के तौर पर कार्यानुभव.