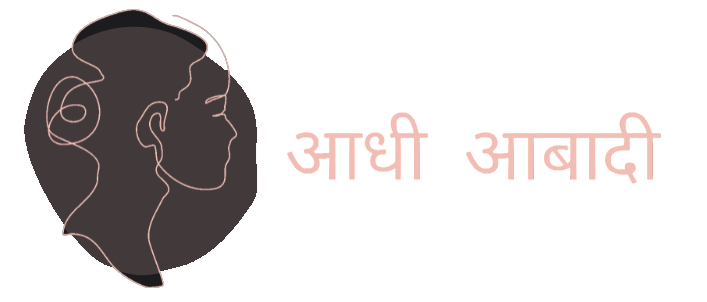डिजिटल शिक्षा की दौड़ में मौलिकता की अहमियत
तकनीक से शिक्षा का विस्तार संभव है, परंतु बच्चों की मौलिकता ही उन्हें यांत्रिकता से बचा सकती है

आज हम शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेज़ी से एक नए माध्यम — डिजिटल माध्यम — की ओर बढ़ रहे हैं। इसे शिक्षा क्षेत्र की लगभग हर समस्या का समाधान मानकर प्रस्तुत किया जा रहा है। जब कोरोना की पहली लहर आई, तब इस चुनौती से निपटने के लिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प अपनाया।
कोरोना की दूसरी लहर में इस विकल्प पर निर्भरता और बढ़ी, लेकिन ऑनलाइन बैठकों, संप्रेषण, संयोजन, और तकनीकी सहयोग में कई चुनौतियाँ थीं। साथ ही, स्कूलों में कंप्यूटर, इंटरनेट और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं की भारी कमी भी सामने आई।
दरअसल, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय और पर्याप्त शिक्षकों की अनुपलब्धता जैसी समस्याएँ पहले से मौजूद थीं, जिनका समाधान अब तक नहीं हो सका है।
स्पष्ट है कि स्कूलों को डिजिटल अध्ययन के लिए सक्षम और सशक्त बनाने हेतु सरकार को बड़े स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि देश के केवल 22% स्कूलों में ही इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है।
तकनीक हर समस्या का रामबाण इलाज नहीं
डिजिटल डिवाइड की अनदेखी और आर्थिक बाधाओं के कारण देश के एक बड़े हिस्से की इस तक पहुँच नहीं है। एनजीओ प्रथम की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में स्कूली शिक्षा से बाहर होने वाले बच्चों का प्रतिशत 5.3 था। इसका प्रमुख कारण कोरोना महामारी रही, जिसने न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी, बल्कि बच्चों को स्कूल से भी दूर कर दिया।
जिन परिवारों के पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर-लैपटॉप नहीं थे, उन्होंने विकल्प के अभाव में बच्चों को स्कूल से निकालना शुरू कर दिया। बच्चे देश के भावी नागरिक हैं, और स्कूल उन्हें लोकतांत्रिक नागरिक बनने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। यदि वे लगातार शिक्षा व्यवस्था से बाहर होते रहे, तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बन जाएगा।
शिक्षा को डिजिटल संसाधनों पर आधारित करना और इन संसाधनों को व्यापक स्तर तक पहुँचाना एक पहलू है। परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि डिजिटल शिक्षा को एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में विकसित किया जाए, मुख्य माध्यम के रूप में नहीं।
भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह देखा गया है कि हर नई तकनीक को समस्या का रामबाण इलाज मान लिया जाता है। हर दौर में कोई नई तकनीक आई है, जिसे शिक्षाविदों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव का वाहक माना है।
लेकिन एक समय के बाद, या किसी नई तकनीक के आने पर, पुरानी तकनीक अप्रासंगिक हो जाती है। यह बार-बार सिद्ध करता है कि शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान इंसानी समझ और विवेक से ही संभव है; तकनीक केवल सहायक की भूमिका निभा सकती है। यह सोचना कि तकनीक हर समस्या का समाधान कर देगी, एक भ्रामक धारणा है।
मौलिकता कभी समाप्त नहीं होती

भारत की आज़ादी के बाद से हर तकनीकी युग — रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर क्रांति या वर्तमान की डिजिटल क्रांति — आम जनता के लिए किसी तिलिस्म जैसा ही रहा है। वे इसे आश्चर्य और भ्रम के साथ देखते हैं, भरोसा करना चाहते हैं, परंतु नहीं कर पाते। प्रौद्योगिकी तक पहुँच के लिए जो सूचना और शिक्षा की खाई है, वह आम आदमी के लिए एक गंभीर बाधा है।
आज देश में सूचनाओं की कोई कमी नहीं है। मात्र चालीस वर्ष पहले तक कुछ ही घरों में अखबार, रेडियो और टेलीविजन हुआ करते थे। आज लगभग हर घर में ये सभी माध्यम मौजूद हैं, और मोबाइल तथा इंटरनेट के साथ पूरा देश सूचनाओं के जाल में घिरा हुआ है। बावजूद इसके, शिक्षा अभी भी आम जनमानस तक उस स्तर पर नहीं पहुँच पाई है।
सरकारों ने तकनीकी संसाधनों को शिक्षा तक पहुँचाने के लिए कई नीतियाँ और योजनाएँ बनाई हैं। हालांकि कुछ संस्थानों तक ही इनकी पहुँच हो पाई है। लेकिन असली प्रश्न यह है कि इस नई तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए, और इसका प्रयोग शिक्षा को किस प्रकार समृद्ध कर सकता है? इन सवालों पर अधिकांशत: कोई ठोस चेतना नहीं दिखती। जब तक संसाधन शिक्षा तंत्र तक पहुँचते हैं, तब तक वे या तो पुराने हो जाते हैं या अप्रासंगिक।
इसका परिणाम यह होता है कि नई चीजें आती हैं और कुछ समय बाद स्टोररूम की शोभा बन जाती हैं। आज देश के कई स्कूलों के स्टोररूम में रेडियो, टीवी, डेस्कटॉप कंप्यूटर आदि धूल खाते देखे जा सकते हैं।
दूसरे शब्दों में कहें, तो शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि तकनीक हर समस्या का समाधान नहीं है। इसके विपरीत, हम तकनीक पर इतनी निर्भर होते जा रहे हैं कि हमारी मानवीय सोच कम होती जा रही है और यांत्रिक सोच हावी होती जा रही है। मानवीय समाज में जीते हुए, मानवीय बने रहना अधिक आवश्यक है, न कि यंत्रवत हो जाना।
नई शिक्षा नीति के कारण डिजिटल माध्यमों पर हमारी निर्भरता बढ़ी है। लेकिन इस निर्भरता के साथ-साथ हमें बच्चों में मौलिकता भी विकसित करनी चाहिए, क्योंकि मौलिकता कभी समाप्त नहीं होती, जबकि मशीनें समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं।
लेखक वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक रह चुके है। संप्रति होम्योपैथी चिकित्सा-पद्धति के जरिए लोगों की सेवा। नई दिल्ली और मुबंई निवास