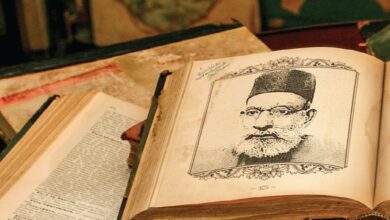“मर्दवादी सोच और महिला हिंसा: समाजीकरण की जड़ों में छिपी क्रूरता”
"कठोर कानून से पहले ज़रूरी है समाज की मानसिकता और पितृसत्ता के ढांचे पर प्रहार"

देशभर ही नहीं, दुनियाभर में, घरेलू और सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं। इस तथ्य से कोई भी सामान्य समझ वाला व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता।
जब महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध मानवीय संवेदनाओं को झकझोरते हैं, तब समाज का एक बड़ा वर्ग कठोर कानूनों की मांग करता है। लेकिन इस मांग के बीच यह सवाल भी उठना चाहिए: क्या केवल सख्त कानून बना देने से महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच में बदलाव आएगा, या फिर वह सोच जस की तस बनी रहेगी?
हर धर्म, जाति और वर्ग हिंसा में शामिल
हर दिन ऐसी अनेक घटनाएं सामने आती हैं, जो यह स्पष्ट करती हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में हर धर्म, जाति और वर्ग के लोग शामिल हैं।
ऐसा लगता है मानो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की एक दौड़ चल रही हो, जिसमें हर समुदाय एक-दूसरे को पीछे छोड़ना चाहता है। कोई भी अपवाद दिखाई नहीं देता।
हाल के वर्षों में एक नई प्रवृत्ति यह भी देखी गई है कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को कभी जाति, तो कभी धर्म के चश्मे से देखा जाने लगा है। इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए दल समाज के सामाजिक सद्भाव को तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह मूलतः पुरुषों द्वारा महिलाओं पर की जा रही हिंसा का मामला है, जिसे गलत तरीके से वर्गीकृत किया जा रहा है।
हर जघन्य घटना के बाद कड़ी सज़ा की मांग उठती है, लेकिन वही समाज इन अपराधों की जड़ में मौजूद सोच को अनदेखा कर देता है—वह सोच, जो इन अपराधों को जन्म देती है।
यह स्पष्ट है कि समाज या तो इन कारणों से अनजान है या जानबूझकर उन्हें नज़रअंदाज करता है। यही कारण है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गई है, जिसे विभिन्न दल अपने-अपने हित में ‘राजनीतिक फुटबॉल’ की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक-दूसरे पर महिला सुरक्षा को लेकर असंवेदनशील होने का आरोप लगाकर, वे अपने-अपने तर्क गढ़ते हैं।
सामाजिक अधिरचना पर चोट जरूरी
महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करने के लिए समाज को अपनी सामाजिक अधिरचना और विशेष रूप से पुरुषवादी सोच पर चोट करनी होगी—वह सोच जो महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है, और उन्हें समानता या स्वतंत्रता के योग्य नहीं समझती।
यह मान लेना गलत होगा कि समाज या समाजशास्त्रियों के पास इसका कोई समाधान नहीं है। वास्तविकता यह है कि समाज ने अब तक इस दिशा में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से नहीं किया है। यदि प्रयास हुए भी हैं, तो वे बेहद सीमित और सतही रहे हैं।
समाज को समाजीकरण की प्रक्रिया को पुनर्परिभाषित करना होगा। उसे यह भाव नष्ट करना होगा कि महिलाएं केवल एक वस्तु या उपभोग की चीज हैं। साथ ही, एक संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास भी आवश्यक है।
प्रसिद्ध नारीवादी सिमोन द बोउआर कहती हैं, “स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है।” उसी तर्ज़ पर यह वाक्य भी उतना ही सत्य है: “मर्दवादी समाज पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है।”
“मर्द को दर्द नहीं होता”, “क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो?”, “मर्द रोते नहीं”, “पुरुष महिलाएं से ज़्यादा मज़बूत होते हैं”—ऐसे जुमले पुरुषों के भीतर एक असंवेदनशील ‘मर्द’ को गढ़ते हैं। इस सोच से जन्मा पुरुष महिलाओं को, चाहे वह बच्ची हो, युवती हो या बुजुर्ग, सिर्फ वस्तु या लोलुपता की दृष्टि से देखता है।
वह उनके साथ किसी भी तरह की हिंसा को जायज़ ठहराने लगता है। उसे लगता है कि जो वर्ग उससे ‘कमज़ोर’ है, उसे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वह कभी कपड़ों, कभी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर ‘फतवे’ जारी करता है। समाजशास्त्र इस प्रवृत्ति को “वर्चस्वशाली मानसिकता” के रूप में परिभाषित करता है।
यदि समाज सचमुच महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनना चाहता है, तो उसे केवल कठोर कानूनों की मांग नहीं करनी होगी, बल्कि अपनी पुरुषवादी सोच और समाजीकरण की प्रक्रिया को भी जड़ से बदलना होगा।
जिस मर्दवादी पुरुष को इस समाज ने अपने समाजीकरण में गढ़ा है, वही असली समस्या की जड़ है। जब तक उस सोच को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाता, तब तक समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित समाज का निर्माण संभव नहीं है—चाहे आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने ही कानून क्यों न बना लें, वे सभी अंततः व्यर्थ साबित होंगे।
यह वेबसाईट आपके ही सहयोग से चलती है।
वेबसाइट को SUBSCRIBE करके
भागीदार बनें।
बेगूसराय, बिहार की रहने वाली अंशू कुमार ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल और पीएचडी पूरी की है। उनकी कविताएँ सदानीरा, हिंदवी, हिन्दीनामा और अन्य पर प्रकाशित हुई है समकालीन विषयों पर उनके लेख नियमित रूप से अखबारों और डिजिटल प्लेटफार्म में पब्लिश होते रहते हैं। वर्तमान में वह अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में रिसर्च फेलो के रूप में कार्यरत हैं।