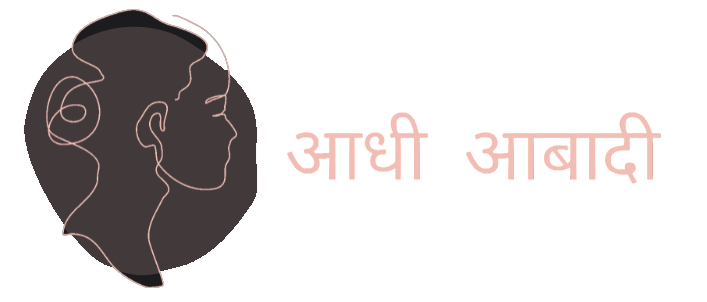पीरियड लीव कोई सुविधा नहीं, महिलाओं का संवैधानिक अधिकार | भारत में कहां और कैसे मिलती है छुट्टी
भारत में महिलाओं के लिए पीरियड लीव कोई विशेष सुविधा नहीं, बल्कि उनका अधिकार है। बिहार देश का एकमात्र राज्य है, जहां 1990 के दशक से महिलाओं को हर महीने दो दिन का पीरियड लीव मिल रहा है।
स्विगी, जोमैटो, बायजूस, एवीपनन, मातृभूमि, मैग्टर, इंडस्ट्रीज, एसीआई, फ्लाईमायबिज़ और गूज़ूप जैसी निजी कंपनियां भी महिला कर्मचारियों को सशुल्क पीरियड लीव प्रदान कर रही हैं। दुनियाभर के कई देशों में भी महिलाओं को इस दौरान अवकाश की सुविधा दी जाती है।
हाल ही में, भारत की सर्वोच्च अदालत में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस विषय पर एक याचिका दायर की गई, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है। यह याचिका इस उम्मीद के साथ दायर की गई है कि महिलाओं को हर महीने आने वाले शारीरिक कष्ट के दौरान कुछ राहत मिल सके। साथ ही, मातृत्व लाभ अधिनियमों को लागू करने हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति की मांग भी की गई है।
भारतीय महिलाओं के लिए पीरियड लीव की मांग कोई नई नहीं है, लेकिन पहली बार यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। महिलाओं के लिए यह सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा मौलिक अधिकार है।
बिहार में कैसे मिला महिलाओं को पीरियड्स लीव का अधिकार

साल 1991 में बिहार राज्य में एक अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई। इस हड़ताल में सरकारी कर्मचारियों ने यह माँग की कि केंद्र सरकार की तर्ज़ पर राज्य में लागू किए गए वेतनमान में मौजूद विसंगतियों को दूर किया जाए।
हड़ताल के दौरान एक चार्टर ऑफ़ डिमांड तैयार किया गया, जिसकी सबसे प्रमुख माँग समान वेतनमान की विसंगतियों को दूर करना थी। इस आंदोलन में स्कूल और विश्वविद्यालय के शिक्षक, बोर्ड और निगमों के कर्मचारी, तथा बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ भी शामिल था।
उसी दौर में महिलाएं विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभा रही थीं। 1985 से ही किसान और मज़दूर अपने अधिकारों और सामंतवाद के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे थे, जिनमें ग्रामीण और निम्नवर्गीय महिलाएं भी जुड़ने लगी थीं। इन आंदोलनों में महिलाओं के मुद्दों पर भी चर्चा होने लगी थी, जैसे—संविधान में प्रदत्त अधिकारों के बावजूद उन्हें वोट देने से वंचित रखना, और पुरुषों के समान मज़दूरी की माँग उठाना।
कामकाजी महिलाएं हॉस्टल और क्रेच जैसी बुनियादी सुविधाओं की माँग भी उठाने लगी थीं। इसी बीच, सरकारी कर्मचारियों का यह हड़ताल भी तेज़ होता जा रहा था। सभी माँगों को सूचीबद्ध किया जा रहा था, तभी हड़ताल में भाग ले रही महिलाओं ने यह माँग उठाई कि पीरियड्स के दौरान उन्हें छुट्टी दी जाए।
उस समय राज्य के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। जब यह माँग उनके सामने रखी गई, तो वे कुछ मिनटों तक मौन रहे और फिर सहमति जताते हुए कहा कि दो दिन की छुट्टी दी जा सकती है। उन्होंने अधिकारियों को इसे नोट करने का निर्देश दिया। यह निर्णय बिहार को पहला ऐसा राज्य बना गया, जिसने महिलाओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी देने का ऐलान किया।
इस फैसले ने महिलाओं के लिए एक नया रास्ता खोला, हालांकि उस समय सामाजिक झिझक और शर्म की दीवारें अब भी कायम थीं। धीरे-धीरे यह सुविधा सामान्य होती गई, और आज बिहार में महिलाओं को पीरियड्स की छुट्टी लेने के लिए कोई कारण या बहाना बताने की ज़रूरत नहीं होती।
यह सवाल आज भी प्रासंगिक है—क्या राज्य सरकारें अपने स्तर पर इस तरह के निर्णय नहीं ले सकतीं?
क्यों ज़रूरी है पीरियड लीव?

दुनिया भर की महिलाओं का पीरियड्स से जुड़ा अनुभव लगभग समान होता है। एक औसत महिला अपने जीवन के लगभग 3,500 दिन—यानी करीब दस साल—पीरियड्स की स्थिति में बिताती है। इनमें से दो साल असहनीय दर्द, रक्तस्त्राव और अन्य समस्याओं से गुजरते हैं। इस दौरान महिलाओं को पेट-दर्द, ऐंठन, उल्टी, चक्कर आना, थकावट, नींद में समस्या, और भावनात्मक अस्थिरता जैसी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यह कोई बीमारी नहीं है, फिर भी यह महिलाओं को अस्वस्थ बना देता है।
ऐसे में अगर महिलाएं इन दिनों में आराम और सहानुभूति की अपेक्षा करें, तो यह कतई अनुचित नहीं है। यह एक मानवीय दृष्टिकोण है, और भारत जैसे देश में इसे अधिकार का रूप देने की आवश्यकता है।
सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1972 के अनुसार पीरियड लीव का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। सरकार पहले से ही महिला कर्मचारियों को अर्जित अवकाश, हाफ-पे लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, चाइल्ड केयर लीव, कम्यूटेड लीव और मैटरनिटी लीव जैसी छुट्टियां देती है। परंतु ये सुविधाएं केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित हैं।
असंगठित क्षेत्र की महिलाओं, विशेषकर घरेलू सहायिकाओं को यह अधिकार नहीं मिल पाता। निजी कंपनियां महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने से भी कतराने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे अतिरिक्त ज़िम्मेदारियां बढ़ेंगी। यही मानसिकता मातृत्व अवकाश के विस्तार के दौरान भी देखने को मिली थी।
समानता की मांग
कुछ राज्य पीरियड लीव दे रहे हैं, कुछ कंपनियां पेड लीव देती हैं, और कई स्थानों पर कोई व्यवस्था नहीं है। इस असमान व्यवहार को समाप्त करने की ज़रूरत है।
कई महिलाएं खुद भी इस अवकाश के खिलाफ हैं, क्योंकि वे नहीं चाहतीं कि उनके पीरियड्स सार्वजनिक हों। ऑफिस में उनके पीरियड्स की गिनती होना शर्मिंदगी और उपहास का कारण बन सकता है। संकीर्ण सोच वाले सहकर्मी भद्दे कमेंट्स और व्यवहार से स्थिति और बिगाड़ सकते हैं।
इन्हीं कारणों से कुछ महिलाएं चाहती हैं कि यह अवकाश उनकी सहमति और सुविधा पर आधारित हो। इसे मेडिकल लीव में शामिल करने का विकल्प भी सुझाया गया है।
महिला अधिकारों की लड़ाई कभी आसान नहीं रही है। पीरियड लीव पर गंभीर और विस्तृत बहस की आवश्यकता है। यह बहस केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और संस्थागत स्तर पर होनी चाहिए। अगर दुनिया के कई देश और कंपनियां इस नीति को अपनाकर बेहतर कार्य-संस्कृति बना सकती हैं, तो भारत में यह क्यों संभव नहीं?
ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि जब सैनिटरी पैड्स को आवश्यक वस्तु मानकर जीएसटी के दायरे से बाहर किया जा सकता है, तो महिलाओं की मूलभूत शारीरिक आवश्यकता के लिए अवकाश देना भी कोई असंभव कदम नहीं है।
बेगूसराय, बिहार की रहने वाली अंशू कुमार ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल और पीएचडी पूरी की है। उनकी कविताएँ सदानीरा, हिंदवी, हिन्दीनामा और अन्य पर प्रकाशित हुई है समकालीन विषयों पर उनके लेख नियमित रूप से अखबारों और डिजिटल प्लेटफार्म में पब्लिश होते रहते हैं। वर्तमान में वह अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में रिसर्च फेलो के रूप में कार्यरत हैं।