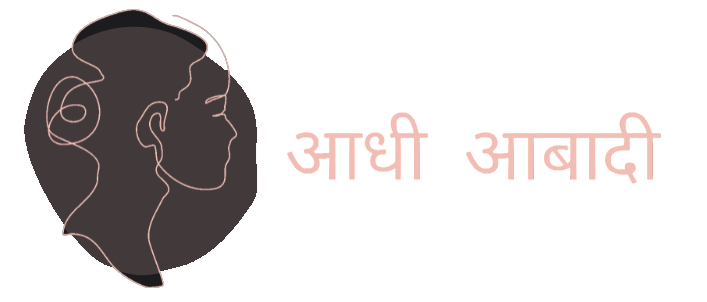जब भी मुस्लिम महिलाओं की बात होती है, तो उनके कपड़ों, विशेष रूप से ‘हिजाब’, ‘बुर्का’ या ‘नकाब’ को चर्चा का केंद्र बना दिया जाता है। कहीं इसे धार्मिक आज्ञा के पालन के रूप में देखा जाता है, तो कहीं इसे पितृसत्तात्मक दबाव और महिला स्वतंत्रता के खिलाफ प्रतीक के रूप में।
क्या पर्दा वाकई एक ‘प्रथा’ है जो महिलाओं पर थोपी जाती है, या यह उनकी ‘चॉइस’ यानी चुनाव की स्वतंत्रता है? और जब मुस्लिम महिलाएं खुद पर्दे का चयन करती हैं, तो वह किस संदर्भ में होता है—धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या सामाजिक?
पर्दा कभी दमन का औजार रहा है, तो कभी प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है।
पर्दा: धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा?
इस्लाम में पर्दा का आधार कुरान की कुछ आयतों और हदीसों पर टिका है, जो महिलाओं से modesty (लज्जा/संयम) के साथ व्यवहार करने को कहती हैं। कई विद्वान मानते हैं कि हिजाब केवल सिर ढकने तक सीमित नहीं, बल्कि यह सम्पूर्ण जीवन शैली है, जिसमें आचरण, चाल-ढाल, भाषा और कपड़े सभी शामिल होते हैं।
पर्दा सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं रहा है। ईसाई मठवासी परंपराएं, यहूदी महिलाओं के सिर ढकने की परंपरा, और यहां तक कि भारतीय हिंदू परिवारों में भी ‘घूंघट’ जैसे रूप देखने को मिलते हैं। यानी पर्दा मूलतः एक सांस्कृतिक परिघटना रही है, जिसे समय और स्थान के अनुसार धर्म ने ढाल लिया।
पर्दा बनाम चॉइस: एक नारीवादी बहस
पर्दा प्रथा को लेकर नारीवादियों के बीच भी बहस बंटी हुई है। एक वर्ग इसे महिलाओं पर थोपा गया पितृसत्तात्मक नियंत्रण मानता है, जो उन्हें सार्वजनिक जीवन, शिक्षा और रोजगार से दूर करता है। वहीं दूसरा वर्ग कहता है कि यदि महिला स्वयं पर्दा चुनती है, तो यह उसकी एजेंसी (स्वायत्तता) का संकेत है।
मसलन, एक मुस्लिम युवती यदि खुद हिजाब पहनकर खुद को ज़्यादा सशक्त, सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती है, तो क्या यह उसके आत्मनिर्णय का उदाहरण नहीं? लेकिन यह भी देखा जाना जरूरी है कि क्या उस चॉइस के पीछे वास्तव में स्वतंत्रता है, या सामाजिक और पारिवारिक दबाव?
विश्व स्तर पर पर्दे पर विवाद और आंदोलन
1. ईरान: हिजाब का प्रतिरोध
1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान में महिलाओं पर हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन समय-समय पर ईरानी महिलाओं ने इसका विरोध भी किया।
2017 में ‘व्हाइट वेडनसडे’ आंदोलन के तहत महिलाएं हर बुधवार को सफेद स्कार्फ पहनकर हिजाब के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने लगीं।
2022 में महसा अमीनी की नैतिक पुलिस द्वारा हिरासत में मौत ने देशभर में विद्रोह को जन्म दिया। “महिला, जीवन, आज़ादी” का नारा अंतरराष्ट्रीय प्रतीक बन गया।
2. फ्रांस और यूरोप में हिजाब पर प्रतिबंध
फ्रांस में 2004 में पब्लिक स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों (हिजाब, क्रॉस, यमकाह) पर प्रतिबंध लगाया गया।
2010 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर भी प्रतिबंध लगा।
इस कदम की आलोचना इस आधार पर हुई कि यह धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी को छीनने का काम कर रहा है।
3. अफगानिस्तान: तालिबानी नियंत्रण
1990 के दशक में और फिर 2021 के बाद, तालिबान के शासन में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से लगभग हटा दिया गया।
शिक्षा, रोजगार, यात्रा सभी पर प्रतिबंध और बुर्का अनिवार्य।
कई महिला कार्यकर्ताओं को जेल, प्रताड़ना और निर्वासन झेलना पड़ा। यह पर्दा नहीं, दमन का नग्न रूप था।
भारत में पर्दा: सांस्कृतिक, राजनीतिक और संवैधानिक बहस
भारत में मुस्लिम महिलाओं के लिए पर्दा एक बहुआयामी मुद्दा रहा है।
हिजाब विवाद – कर्नाटक, 2022
उडुपी के एक कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षाओं में आने से रोका गया, जिसके खिलाफ छात्राओं ने अदालत और सड़कों दोनों पर संघर्ष किया। मामला धार्मिक स्वतंत्रता बनाम संस्थागत अनुशासन के बीच फंस गया।
सुप्रीम कोर्ट में भी यह मुद्दा पहुंचा, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत में मुस्लिम महिलाओं की चॉइस आज भी चुनौतीपूर्ण राजनीतिक और कानूनी बहस में फंसी हुई है।
भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में पर्दा एक सामाजिक मानदंड है। कई परिवारों में बिना पर्दे के घर से निकलना ‘बदतमीज़ी’ माना जाता है। लड़कियों को कम उम्र से ही बुर्का पहनने को कहा जाता है ताकि वे “इज्जतदार” बनें।
चॉइस की सीमाएं: पर्दा सिर्फ ‘कपड़ा’ नहीं है
यह मानना एक भूल होगी कि हिजाब या पर्दा सिर्फ एक फैशन या निजी निर्णय है। जब एक महिला हिजाब पहनती है, तो वह समाज में एक ‘धार्मिक पहचान’ दर्शाती है — जो उसे भेदभाव, टिप्पणियों, या राजनीतिक शक का शिकार भी बना सकती है। वहीं अगर कोई महिला हिजाब नहीं पहनती, तो वह अपने समुदाय से उपेक्षा, तिरस्कार या ‘गैर-मुस्लिम’ कहे जाने का खतरा झेल सकती है।
यानी ‘चॉइस’ का होना और ‘चॉइस’ का सम्मान होना — दोनों अलग बातें हैं।
क्या पर्दा प्रतिरोध का भी प्रतीक बन सकता है?
जी हां। कई महिलाओं ने पर्दे को औज़ार बनाया है:
पर्दा या चॉइस — असली मुद्दा ‘एजेंसी’ है
पर्दा प्रथा बनाम चॉइस की बहस में हमें यह समझने की ज़रूरत है कि असली मुद्दा पर्दा नहीं, बल्कि एजेंसी है। क्या महिलाएं अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद फैसले ले पा रही हैं? यदि कोई महिला पर्दा करती है, लेकिन उसे न करने की आज़ादी भी हो — तो वह चॉइस है। यदि उसे पर्दा उतारने की स्वतंत्रता नहीं, या पहनने पर समाज द्वारा कलंकित किया जाए — तो वह चॉइस नहीं, दबाव है।
‘चॉइस’ तभी असली होती है जब विकल्प भी बराबर हों और उनके साथ जीने की इज्जत और सुरक्षा भी। आज की महिलाएं सिर्फ पर्दे या बेपर्दगी के बीच नहीं फंसी हैं। वे पहचान, सुरक्षा, आत्मसम्मान, धर्म और समाज के बीच अपनी राह बना रही हैं। पर्दा उनके लिए कहीं दमन है, कहीं प्रतिरोध, और कहीं आत्म-अभिव्यक्ति का ज़रिया।
हमें ज़रूरत है एक ऐसे समाज की, जहां कोई महिला चाहे तो हिजाब पहने, चाहे तो न पहने — और दोनों ही स्थितियों में वह बराबर इज्जत, आज़ादी और अवसर की हकदार हो।
मेरी कलम मेरे जज़्बात लिखती है, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, उनके अल्फाज़ लिखती है। Received UNFPA-Laadli Media and Advertising Award For Gender Senstivity -2020 Presently associated with THIP- The Healthy Indian Project.