“सोशल मीडिया: लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी और दुरुपयोग की नई चुनौतियां”
"जहां सोशल मीडिया संवाद का मंच था, वहीं अब यह दुष्प्रचार और उत्पीड़न का ज़रिया बनता जा रहा है"
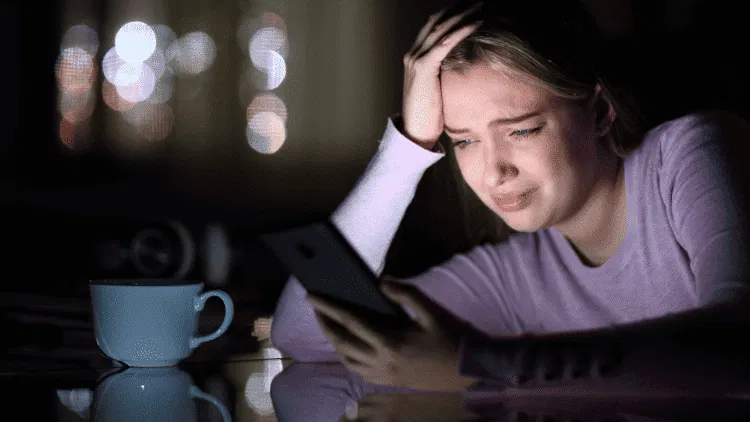
सोशल मीडिया मंचों को एक ऐसा माध्यम माना गया था, जहां लोग आसानी से एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। यह विश्वास था कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिलेगी।
आज भी सोशल मीडिया सामाजिक मुद्दों को उजागर करने, सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देने और राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है।
हालांकि, इसके बावजूद मौजूदा समय में सोशल मीडिया के नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन को लेकर एक गंभीर दुविधा उत्पन्न हो गई है।
एक ओर चीन जैसे देशों में सोशल मीडिया पर सख़्त पाबंदियां हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश है। वहीं, दूसरी ओर लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार माना जाता है और लोगों को अपनी राय रखने की पूरी छूट है।
आज सोशल मीडिया हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है।
शुरुआत में सोशल मीडिया को संवाद, बहस और गंभीर विमर्श का मंच माना गया था, लेकिन जैसे-जैसे इसकी पहुंच बढ़ी, इसका दखल हमारी दिनचर्या में भी गहराई से पैठ गया। समय के साथ इसका दुरुपयोग बढ़ता गया, और यह मंच धमकाने, उत्पीड़न करने, दुष्प्रचार फैलाने, फर्ज़ी ख़बरों के प्रचार, सामाजिक तानेबाने को कमजोर करने और विदेशी हस्तक्षेप का माध्यम बनने लगा।
अब सोशल मीडिया का उपयोग कई बार हिंसा भड़काने, लोगों को उकसाने, अशांति पैदा करने और ग्रे-ज़ोन युद्ध जैसी गतिविधियों में भी किया जा रहा है। यही कारण है कि इन मंचों की गतिविधियों पर नियंत्रण, अभिव्यक्ति की सीमाओं का निर्धारण और इसे कानून के दायरे में लाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
सैद्धांतिक रूप से सोशल मीडिया को सामाजिक, नागरिक और राजनीतिक भागीदारी के मंच के रूप में सुरक्षित और संरक्षित बनाए रखना चाहिए। परंतु, प्रायः अनजाने में या कभी-कभी जानबूझकर, इन मंचों पर लोगों की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित कर दिया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव की चेतावनी
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 2023 में चेतावनी दी थी कि:
“ऑनलाइन माध्यमों पर नफ़रत और फर्जी सूचनाओं का प्रसार हमारी दुनिया को गंभीर क्षति पहुँचा रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए भ्रामक और नफरत फैलाने वाली सामग्री पूर्वाग्रह, हिंसा और सामाजिक विभाजन को बढ़ा रही है। साथ ही यह अल्पसंख्यकों की छवि को बिगाड़ने और चुनावों को प्रभावित करने का ज़रिया बन गई है।”
इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो गया है कि विचारों की स्वतंत्रता और डिजिटल सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। दुनिया भर की सरकारें इस दिशा में प्रयासरत हैं और नीतिगत तथा कानूनी उपायों के माध्यम से समाधान तलाश रही हैं।
सोशल मीडिया और महिलाओं की भागीदारी में गिरावट
सोशल मीडिया भले ही एक लोकतांत्रिक मंच के रूप में सामने आया हो, लेकिन महिलाओं के लिए यह स्थान हमेशा सुरक्षित नहीं रहा। विशेष रूप से विकासशील देशों में महिलाएं ऑनलाइन माध्यमों पर असमानता, उत्पीड़न, ट्रोलिंग, अश्लील टिप्पणियों और निजता के उल्लंघन जैसी समस्याओं का सामना करती हैं।
हाल के वर्षों में कई महिलाएं सोशल मीडिया से दूरी बना रही हैं या अपनी उपस्थिति को काफी सीमित कर रही हैं। यह डिजिटल बहिष्करण महिलाओं की आवाज़ को सार्वजनिक विमर्श से बाहर करता है और लोकतांत्रिक भागीदारी को कमजोर करता है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशन्स वीमेन के अनुसार, हर तीन में से एक महिला को सोशल मीडिया पर हिंसात्मक या धमकी भरे अनुभव होते हैं।
जब महिलाएं राजनीतिक या सामाजिक मुद्दों पर राय रखती हैं, तो उन्हें अक्सर ट्रोलिंग, यौन उत्पीड़न और धमकियों का सामना करना पड़ता है। इस डर और असुरक्षा के कारण महिलाएं या तो चुप हो जाती हैं या मंच ही छोड़ देती हैं।
समाधान की दिशा में व्यापक सुझाव
1. सोशल मीडिया कंपनियों की ज़िम्मेदारी बढ़ाना
- “मध्यस्थ दायित्व” की अवधारणा को मजबूत करना, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने होस्ट किए गए कंटेंट के लिए उत्तरदायी बनें।
- आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए प्रशिक्षित टीम और उन्नत तकनीकी समाधानों का उपयोग सुनिश्चित करना।
2. पोस्ट-चेकिंग और सूचना सत्यापन
- राष्ट्रीय डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम में सत्यापन की व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
- एक स्पष्ट आचार संहिता और मानक संचालन प्रक्रियाएं बनाना और सख्ती से लागू करना।
3. सोशल मीडिया शासन के लिए स्पष्ट तंत्र
- सामुदायिक दिशा-निर्देश और मौजूदा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना।
- प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयुक्त नियम-कानून विकसित करना ताकि समस्या का व्यापक समाधान हो सके।
4. नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना
- यूज़र्स को मंच के नियंत्रण में भागीदार बनाना, जिससे पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो।
- कंपनियों को भागीदारी को केवल प्रतीकात्मक न रखकर नीतिगत रूप से शामिल करना होगा।
5. ऑनलाइन खतरों की पहचान और मानक
- वैश्विक स्तर पर सोशल मीडिया कंपनियों के संचालन के लिए एक समान नियामक ढांचा विकसित करना।
- ऑनलाइन खतरों की पहचान के लिए स्पष्ट मानदंड तय करना।
6. AI-संचालित निगरानी प्रणालियों को विकसित करना
- स्थानीय भाषाओं में पोस्ट किए गए आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान के लिए एआई टूल्स विकसित करना।
- हितधारकों के सहयोग से व्यापक स्तर पर डेटा संग्रहण और विश्लेषण करना।
सोशल मीडिया को सुरक्षित, उत्तरदायी और समावेशी बनाया जाए
सोशल मीडिया एक तरफ जहां लोकतांत्रिक मूल्यों के पोषण का मंच बन सकता है, वहीं दूसरी ओर इसके दुरुपयोग से सामाजिक विभाजन और हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है।
खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए यह मंच चुनौतियों से भरा हुआ है। अतः ज़रूरत इस बात की है कि इस माध्यम के प्रयोग को सुरक्षित, उत्तरदायी और समावेशी बनाया जाए।
सही नीतियों, तकनीकी समाधानों, और व्यापक जनभागीदारी के साथ सोशल मीडिया को एक सकारात्मक और रचनात्मक माध्यम के रूप में पुनः स्थापित किया जा सकता है।
यह वेबसाईट आपके ही सहयोग से चलती है।
वेबसाइट को SUBSCRIBE करके
भागीदार बनें।
मेरी कलम मेरे जज़्बात लिखती है, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, उनके अल्फाज़ लिखती है। Received UNFPA-Laadli Media and Advertising Award For Gender Senstivity -2020 Presently associated with THIP- The Healthy Indian Project.




