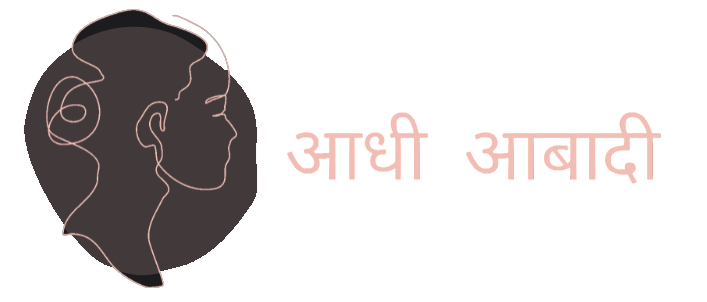अम्मू स्वामीनाथन : संविधान सभा में महिला अधिकार को बुलंद करने वाली थीं

किसी स्कूल-कालेज में शिक्षित नहीं होने के बाद भी अम्मू स्वामीनाथन एक महिला नहीं, कई संभावनाओं की कहानी हैं, वह संभावना, जो तमाम महिलाओं में दबकर रह जाती है।
‘बाहर के लोग कह रहे हैं कि भारत ने अपनी महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं दिए हैं। अब हम कह सकते हैं कि जब भारतीय लोग स्वयं अपने संविधान को तैयार करते हैं तो उन्होंने देश के हर दूसरे नागरिक के बराबर महिलाओं को अधिकार दिए हैं।’
24 नवंबर 1949 को संविधान के मसौदे को पारित करने के लिए डॉ बी आर अम्बेडकर की एक चर्चा के दौरान भाषण में आशावादी और आत्मविश्वासी अम्मू स्वामीनाथन ने कहा था। संविधान तैयार करने के लिए 425 सदस्यीय संविधान समिति का चुनाव किया गया था जिसमें केवल 15 महिलाएं ही थीं, अम्मू स्वामीनाथन उनमें से एक थी।
अम्मू स्वामीनाथन अपनी मां के घर में पली बढ़ी थीं
अम्मू का जन्म केरल के पालघाट जिले के अनाकारा में ऊपरी जाति के हिंदू परिवार में 22 अप्रैल 1894 में हुआ था। वह अपनी मां के घर में पली बढ़ी थी। सबसे छोटी होने के कारण बहुत लाडली भी थी।
पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी तो मां परिवार की मुखिया थी और उनके मज़बूत व्यक्तित्व का असर अम्मू पर पड़ा। घर के दूर केवल लड़कों को पढ़ने भेजा जाता था, इसलिए अम्मू स्कूल नहीं गई। उन्हें घर पर ही मलयालम में थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला।
13 साल के उम्रं में अम्मू की मुलाकात स्वामीनाथन नाम के वकील से हुई। बचपन में अम्मू के पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उनकी मदद की थी। छात्रवृत्तियों के सहारे स्वामीनाथन को देश-विदेश में पढ़ने का अवसर मिला और उन्होंने मद्रास में वकालत शुरू कर दी। जब उन्होने घर बसाने की सोची, तो मदद करने वाले अम्मू के पिता को याद किया। स्वामीनाथन ने अपना प्रस्ताव अम्मू की मां के सामने रख दिया – अगर उनकी बेटी शादी के लायक हो, तो वह उससे शादी करने के लिए उत्सुक है।
अम्मू से जब पूछा गया? अम्मू तैयार हो गई पर शर्त्त रख दी मैं गांव में नहीं, शहर में रहूंगी और मेरे आने-जाने के बारे में कोई कभी सवाल न पूछे। स्वामीनाथन ने सारी शर्ते मान ली। उस जमाने में ब्राह्मण की शादी नायर महिला से नहीं होता था। इस शादी का ब्राह्मण समाज में काफी विरोध हुआ।
स्वामीनाथन ने अम्मू से शादी की, विलायत जाकर कोर्ट मैरिज भी की और अम्मू स्वामीनाथन हो गई। जिस तरह से अम्मू ने अपने पति के समक्ष अपनी इच्छा वयक्त की उससे तय हो जाता है कि अम्मू बचपन में ही एक आत्मविश्वासी और जोश से भरी हुई लड़की थी। स्वामीनाथन एक पति के तरह ही नहीं एक मार्गदर्शक के तरह अम्मू के जीवन में आए। उन्होंने अम्मू के लिए टूयूशन लगवाई और उन्हें अग्रेजी लिखना-पढ़ना सीखाया।
अम्मू स्वामीनाथन अपने पति से भी आगे निकल गई
एक समय आया कि अम्मू अपने पति से भी आगे निकल गई और लोगों से बेझिझक बातचीत करने लगी। अम्मू ने लैंगिक और जातिगत उत्पीड़न का हर स्तर पर विरोध किया। वह हमेशा मानती थी कि नायर एक पिछड़ी जाति है इसलिए नायर समुदाय में महिलाओं को जातिगत और लैंगिक दोनों ही उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।नायर समुदाय के होने के कारण अम्मू ने जातिगत उत्पीड़न को करीब से देखा था।
औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं करने के बाद भी अम्मू ने समाज में महिलाओं के दोयम स्थिति की पहचान बचपन में ही कर ली थी, जब उन्हें घर में ही अपनी पारंपरिक शिक्षा पूरी करनी पड़ी, जबकि केरल में मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था कायम है।
साल 1917 में मद्रास में एनी बेसेंट, मार्गरेट, मालथी पटवर्धन, श्रीमती दादाभाय और श्रीमती अंबुजमल के साथ महिला भारत संघ का गठन किया। इस मंच के सहायता से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक स्थितियों के जिम्मेदार कारणों पर अपनी आवाज बुलंद करने का काम किया।
अम्मू सबसे अधिक सक्रिय स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में रहीं

अम्मू साल 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बन गई। वह साल 1952 में लोकसभा के लिए और साल 1954 में राज्यसभा के लिए चुनी गयी। वह भारत स्काउट्स एंड गाइड (1960-65) और सेंसर बोर्ड की भी अध्यक्ष भी रही। स्त्री शिक्षा वह क्षेत्र है जहां अम्मू सबसे अधिक सक्रिय रही।
किसी स्कूल और कालेज में शिक्षित नहीं होने के बाद भी अम्मू स्वामीनाथन एक महिला नहीं, कई संभावनाओं की कहानी है। वह संभावना, जो तमाम महिलाओं में दबकर रह जाती है क्योंकि अनुकूल परिस्थितियों और वातावरण में प्रतिभा, हुनर सब के सब बिखर जाते है।
नेहरूजी के पंडित जी कहलाने पर नोक-झोक
अम्मू ने अपने वैवाहिक जीवन में जातिवाद का गहरा दंश झेला था, नायर जाति के होने के कारण। उनकी बेटियों को घर के बरामदा में खाना खाने की अनुमति नहीं थीं क्योंकि उनके पति के परिवार के अनुसार वे संपूर्ण ब्राह्मण नहीं थी। इसका विरोध अम्मू ने जीवनभर किया और इसतरह के रीतियों के खिलाफ अभियान भी चलाया।
इसलिए उन्होंने पंडित जी कहलवाने पर नेहरूजी की भी निंदा की थी क्योंकि यह टाइटल उनके उच्च जाति को दर्शता था। हालांकि बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी वजह दी थी कि वह किसी से पंडित कहने को नहीं कहते, लोग उन्हें कहते हैं पर फिर भी अम्मू को इस बात से परेशानी थी कि वो पंडित जी कहे जाने पर कोई प्रतिक्रिया क्यों देते हैं?
4 जुलाई 1978 को केरल में उनका निधन हुआ। उनका पूरा जीवन गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजबूत प्रेरणा देता है। साथ ही साथ अपनी बात को मुखरता से कहना, आपके व्यक्तित्व को असीम संम्भावनाओं से भर सकता है। वह संम्भावनाएं जो एक आम स्त्री के अंदर दबकर रह जाती है।
किसी भी व्यक्ति का परिचय शब्दों में ढले, समय के साथ संघर्षों से तपे-तपाये विचार ही दे देते है, जो उसके लिखने से ही अभिव्यक्त हो जाते है। सम्मान से जियो और लोगों को सम्मान के साथ जीने दो, स्वतंत्रता, समानता और बधुत्व, मानवता का सबसे बड़ा और जहीन धर्म है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने वर्तमान और भविष्य में भी इन चंद उसूलों के जीवन जी सकूंगा और मानवता के इस धर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ पाऊगा।