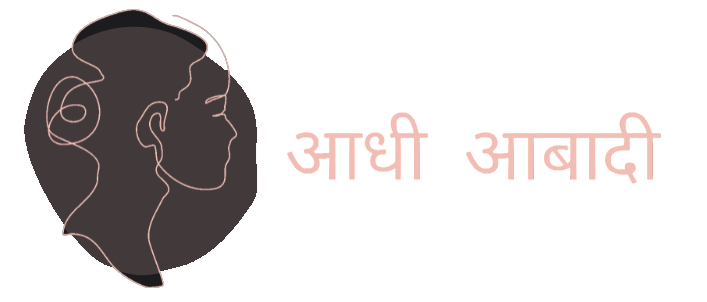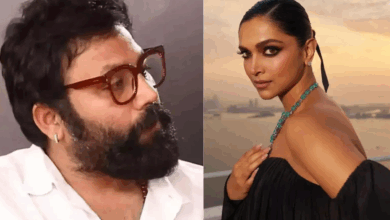महिलाओं के जीवन को आसान बनाने वाले आधुनिक आविष्कार

आधुनिक मानवीय सभ्यता में कुछ नए आविष्कार हुए हैं, जिसकी वजह से महिलाओं की दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान सरलतापूर्वक संभव हो सका है। सस्ते और प्रभावी आविष्कार जो महिलाओं की दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान बने।
मानवीय सभ्यता के कमोबेश हर चरण में “आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है” के जुमले ने एक से बढ़कर एक शानदार आविष्कार किए, जिसने मानवीय जीवन को सहज और आरामदायक बनाने की कोशिशे की है।
तमाम हो चुके आविष्कार में और हो रहे नए आविष्कार में जिसका मानवीय सरोकार अधिक होता है उनको विशेष महत्व दिया जाता है। उन विशिष्ट आविष्कारों में वह आविष्कार जिन्होंने स्त्री-पुरुष के बंटे दुनिया के वर्ग में स्त्री जीवन के संघर्ष को, खासकर उनके दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को समान्य किया हो उसका महत्व महिलाओं के लिए अलग तरह होता है।
कहते है सिंगर कंपनी के संस्थापक जिन्होंने सिलाई मशीन का आविष्कार किया, वह अपनी पत्नी को सुई से कपड़ों की सिलाई करने के दौरान सुई के उगुलियों में चुभने और खून निकलने से अधिक परेशान हो गए। उनकी पत्नी को होने वाली पीड़ा को ना देख पाने के भाव ने उनसे सिलाई मशीन की खोज करवा दिया।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी अपनी किताब “हिंद स्वराज” में मशीनों के उपयोग के संबंध में एक अलग विचार रखते हैं परंतु जो मशीन मानवीय जीवन में महिलाओं के जीवन को सरल-सुलभ बना सके, उसका पुरजोर समर्थन भी करते हैं।
उसी तरह आधुनिक होती मानवीय सभ्यता में कुछ नवीनतम आविष्कार हुए हैं, जिसकी वजह से महिलाओं की दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान सरलतापूर्वक संभव हो सका है। बस इन आविष्कारों का महिलाओं तक पहुंचने भर की देर है।
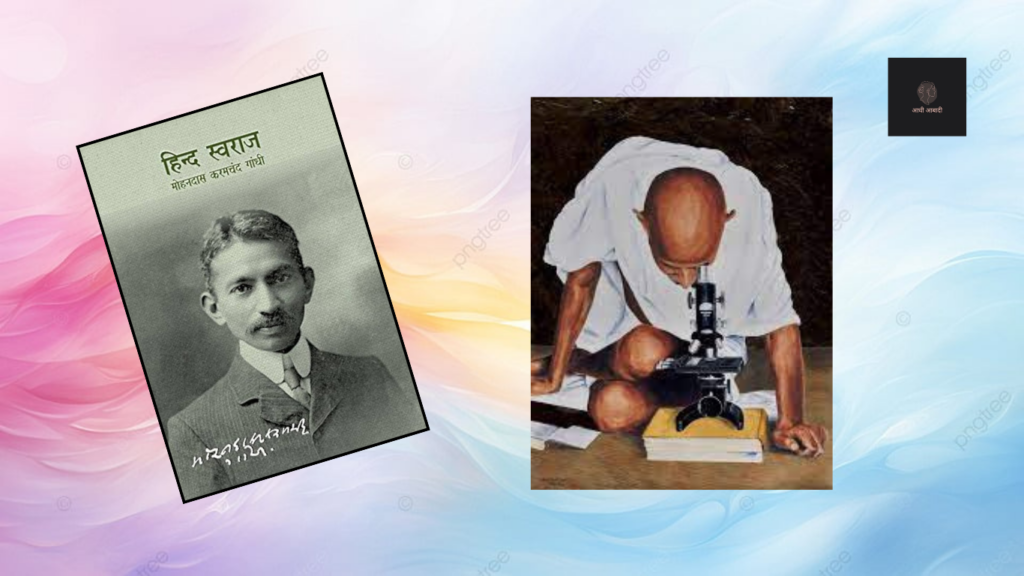
महवारी में इंफेक्शन एंव अन्य बीमारियों से सुरक्षा के सस्ता सेफ्टी किट
रवांडा में कम से कम 18 फीसदी छात्राएं या कामकाजी महिलाएं हर साल करीब 35 दिनों तक स्कूल या दफ्तर नहीं जा पाती थी। इसकी वज़ह यह थी कि मंहगे सैनटरी पैड्स या खरीदना उनके बूते की बात नहीं। इन्हें असुरक्षित विकल्प अपनाने पड़ते थे।
इनके दर्द और तकलीफ को समझा यहां की संस्था सस्टेनेबल हेल्थ एंटरप्राइज ने। हार्वड बिजनेस स्कूल की ग्रेजुएट एंव संस्था की संस्थापक एलिजाबेथ स्कार्फ ने केले के पेड़ के फाइबर्स से एक सस्था पैड बनाया जिसकी कीमत मात्र दो रुपए है।
दूर-दूर से पानी लाने की मजबूरी का समाधान क्यू ड्रम
पानी की समस्या, मानवीय जीवन की वह समस्य है जिसके अभाव में जीवन की कल्पना मुश्लिल है। दक्षिण अफ्रीका में दूर-दूर से महिलाओं को पानी लाने के लिए जाना पड़ता था।
दो भाइयों हैंस और पीट हैण्ड्रीक्स ने महिलाओं को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए पोलीथिलीन से मजबूत “क्यू ड्रम” बनाया, जिसमें 50 लीटर पानी या अनाज वगैरह आसानी से भर कर कठिन से कठिन सड़क पर भी लुढ़का कर लाया जा सकता है। इसी “क्यू ड्रम” का इस्तेमाल आज पानी के संग्रहण या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता है।
इसने दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं दुनिया के कई भागों में जहां पानी की समस्या है वहां एक माकूल समाधान दिया है। खासकर महिलाओं को जो दूर-दूर से पानी संग्रहीत करके लाती थी और वो कम पड़ जाता था।

सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते प्रकोप को जानने के लिए विनेगर टेस्ट
अमरीका के बाल्टीमोर स्थित होपकिंग्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर “झपियेगो” नामक एक गैर सरकारी संस्थान ने आसान मगर उपयोगी तकनीक ईजाद की है। ज़रा से प्रशिक्षण के बाद कोई भी इस डायग्नोस्टिक तकनीक की मदद से समय रहते हुए सर्वाइकल कैंसर का पता लगा सकेगा।
इस तरह इस रोग से होने वाली मृत्यु दर को घटा कर 33 फीसदी पर समेटा जा सकता है। इस तकनीक में सामान्य सिरके की मदद से बीमारी का पता लगाया जा सकता है।
भोजन पकाने में वायु प्रदूषण से बचने के लिए ग्रीन स्टोव का प्रयोग
लकड़ी कोयला जैसे ईधनों के उपयोग से जहरीली गैस का उत्सर्जन होता है। जिससे महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कत आती है क्योंकि रसोई बनाने की अधिकांश जिम्मेदारी महिलाओं के जिम्मे होती है। अनुमान के मुताबिक चार मिलियन लोग अकाल मृत्यु के शिकार होती है जिसकी वज़ह जहरीली गैस है।
दक्षिण अफ्रीका की कम्पनी अफ्रीकन क्लीन एनर्जी के एक ग्रीन स्टोव बनाया है, जो 70 फीसदी कम ईधन का प्रयोग करता है और 95 फीसदी कम जहरीली गैस का उत्सर्जन करता है। यह बैटरी से चलता है, जिसे सौर ऊर्जा से चार्ज कर सकते हैं।
घरेलू प्रसव में महिलाओं के मृत्यु के समस्या से निपटने के लिए सेफ्टी किट
प्रसव के दौरान महिलाओं की सबसे ज्यादा मृत्यु की मार झेलने वाले देश बांग्लादेश के एक समाजसेवी संगठन “बीआरएससी” ने सुरक्षित घरेलू प्रसव के लिए मात्र 25 रुपए की कीमति वाला होम डिलीवरी किट बनाया है।
कल्याणी नामक इस सेफ्टी किट में गांज पट्टी, इंफेक्शन दूर करने वाला कार्बोलिक साबुन, एक स्टराइल प्लास्टिक शीट, सर्जिजल ब्लेड और धागे की गिट्टी दी गई है। इस किट के उपयोग से घरेलू प्रसव को काफी हद तक सुरक्षित बनाया जा सकता है।
बस इन नए आविष्कार की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुंचने भर की देर है।
मेरी कलम मेरे जज़्बात लिखती है, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, उनके अल्फाज़ लिखती है। Received UNFPA-Laadli Media and Advertising Award For Gender Senstivity -2020 Presently associated with THIP- The Healthy Indian Project.